
सुबह जानीमानी पत्रकार राधिका रामासेशन ने ट्विटर पर सवाल उठाया कि बाल अधिकारों के चैम्पियन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने फिलिस्तीन में मारे जा रहे बच्चों पर एक भी शब्द कहा क्या ?
यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आंकड़ों के मुताबिक़ हर रोज साढ़े चार सौ बच्चे फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं।
शाम को भारत के उन बेघर बच्चों का खेला नाटक 'चिड़िया मुझे बना दे राम' देखा, जो या तो दिल्ली के रैन बसेरों में रहते हैं या अस्थाई झुग्गियों में।
नाटक देखते हुए सुबह पढ़ा राधिका रामसेशन सवाल यही समझाता रहा कि बच्चों के cause का चैम्पियन होना एक बात है, उनके जीवन में सार्थकता का अहसास भरना, उन्हें मानवीय गरिमा का भान होना और उनके भीतर की रचनात्मकता को चिन्हित करना बिलकुल दूसरी बात है। यह दूसरी बात यथास्थितिवादियों और दयालुदानियों की व्यापक योजनाओं में फिट नहीं बैठती क्योंकि एक तो उसमें जीवन खपाना होता है दूसरे इससे असहज करने वाले सवाल खड़े होते हैं जिनका निदान शोषण पर खडी व्यवस्था की जड़ें हिला देगा।

दिल्ली के श्रीराम सेंटर सभागार में कल शाम बड़ी संख्या में वो बच्चे और किशोर किशोरियां भी शामिल थे जो अपने दोस्तों और साथियों का नाटक 'चिड़िया मुझे बना दे राम' देखने जुटे थे। नाटक का शीर्षक देखकर पहला विचार मन में आता है कि यह कोई 'पंख होते तो उड़ जाती रे' जैसी मध्यवर्गीय आकांक्षा भर का भाव पेश करता होगा लेकिन वहां मंच पर लगभग 30 बच्चो की फ़ौज थी जिनकी उम्रें 8 साल से 16 साल के बीच रही होंगी और जिनके लिए 'चिड़िया मुझे बना दे राम' कोई याचना और अभ्यर्थना का दूसरा नाम नहीं थी बल्कि उनके चेहरे अनिश्चय, रोष और विश्वास से भरे थे।
उस पर भी कमाल यह कि उन्हें नाइंसाफियों, विद्रूपताओं और क्रूरताओं को सभी प्रचलित नाटकीय प्रविधियों के बीच से कहना था। इसके लिए अभिनय, संवाद, प्रकाश, गीत, संगीत, नृत्य, रूप और वस्त्र सज्जा के स्थापित उपकरणों का अपने हित में इस्तेमाल करना था।

नाटक ने अपनी शुरुआत के साथ ही यह भरोसा जता दिया कि उसका स्वर कला के नखरीले और विगलित स्कूल का नहीं है बल्कि जकड़न, स्वप्न और मुक्ति की आकांक्षा का चीत्कार है। जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो इस खतरे से बेखबर नहीं हूँ कि इन पंक्तियों का पाठक नाटक को वर्गीय प्रतिरोध का नारा न समझ ले। जबकि यह दुहराना ज़रूरी है कि नाटक अपने उन सारे ज़रूरी लेकिन जोखिम भरे उपादानों से अपनी बात कहने की राह पर कामयाबी से तब तक चलता रहा जहां वह एक दृश्य उपस्थित हुआ जब मंच के समूचे विस्तार के बीचोबीच एक बड़े से बासी भगौने के भीतर बैठा एक छोटा सा बच्चा ईंट के अद्धे से उसकी तलछट साफ़ कर रहा है।

ईंट से भगौने के घिसने की एक कर्णकटु ध्वनि बार-बार आपको यह सोचने को मजबूर करती है कि क्या वह उस काई को खुरचने की कोशिश कर रहा है जो व्यापक रूप से संवेदनाओं पर जमती जा रही है ? क्या वह संसार रूपी मंच के केंद्र में रखी खाली व्यवस्था को मांजता हुआ उसके बनाए नियमों और स्वीकार्यताओं की कर्कशता से हमारी नींद उड़ा देना चाहता है ? अभी हम यह सोच ही रहे होते हैं कि बच्चा बीच-बीच खुरचना रोककर उत्तरोत्तर जो इच्छाएं जाहिर करता है वे जैसे किसी घोषणापत्र की तरह पूरे ध्वनिपटल पर छा जाती हैं।

गौर करने पर पता चलता है कि वे बेहद मामूली इच्छाएं हैं जिन्हें तो कब का पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन जिन्हें न्याय, धर्म और राजनीति के घोषणा पत्रों ने कभी जगह ही नहीं दी। बच्चा इन मासूम इच्छाओं से भरे लम्बे संवाद के साथ साथ अपने स्थान पर उठा खड़ा होता है। वह अब भी बोल रहा है और ईंट का घिसा हुआ अद्धा पकडे उसका हाथ क्रमशः हवा में उठता है और अब वह सभ्यता और विकास के वृत्त में खड़ा एक मुश्किल सवाल बन गया है। मेरे लिए नाटक का यही वह पल था जब नाटक का पर्दा गिर जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद लगभग आधे घंटे नाटक और चला जिसके लिए मैंने अपने कान फेर लिए और नजरें झुका लीं।
नाटक के निर्देशक लोकेश जैन और जमघट समूह का मैं आभारी हूँ कि यह अनोखा अनुभव मेरे हिस्से आया। लाइटिंग के लिए हिमांशु को विशेष बधाई।
irfan | 01 November, 2023










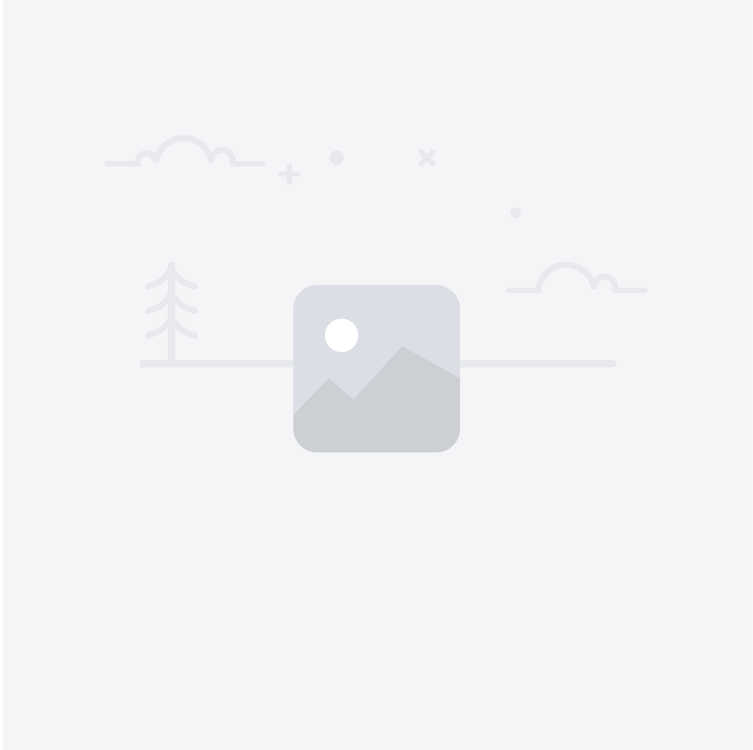










Write a comment ...