
"फिल्म बदनाम में उल्हास और मुराद भी महत्वपूर्ण रोल कर रहे थे। दोनों की जबान पर सरस्वती विराजमान थी। उन्हें सैकड़ों-हजारों की संख्या में शेर याद थे। हिंदी-उर्दू उनकी मातृभाषा थी। जब वे शराब के गिलास भरकर एक दूसरे से चोंचबाजी करने लगते, तो सुननेवालों पर जादू सा तारी हो जाता। इसी तरह, केएन सिंह, हमीद बट, कामेश्वर सहगल, कन्हैयालाल और बद्रीप्रसाद जैसे कलाकारों के मुंह से भी मैं शब्दों की फुलझड़ियां छूटती हुई देखता और महसूस करता कि मैंने बीबीसी की नौकरी के जमाने में यद्यपि हिंदी-उर्दू पर बेहद मेहनत की थी पर फिल्मी कलाकार कहलाने का मैं तभी हकदार हो सकता हूं, जब मैं इन लोगों जैसी सहजता, रवानी और सुंदरता के साथ हिंदी बोल सकूंगा। अभिनय के मामले में मैं आवाज से ज्यादा खेलने का हिमायती नहीं था, पर यह जरूर मानता था और आज भी मानता हूं कि जिस भाषा में अभिनेता बनना हो - उसका, उसके उच्चारण का, उसकी शब्दावली का और साहित्य का आदमी को माहिर होना चाहिए वरना उसका विकास एक जगह पर आकर रुक जाने का खतरा है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं लगातार अभ्यास करता था और मुझे सफलता भी जरूर मिलती थी पर फिर भी उल्हास या मुराद तक पहुंचने की आशा, मैं एक जन्म में तो क्या, दो जन्मों में भी नहीं कर सकता था। मुझे अपनी मातृभाषा पंजाबी की ओर प्रेरित करने के लिए उल्हास और मुराद का बहुत सा हाथ है।"
(बलराज साहनी, मेरी फिल्मी आत्मकथा, दूसरा दौर अध्याय 6)

यहां लिखे नामों में एक नाम कन्हैयालाल का भी है जो फिल्मकार महबूब की औरत (1940) में भी शोषक साहूकार बने थे और बाद में जब इसी फिल्म को उन्होंने दुबारा मदर इंडिया (1957) नाम से बनाया तो उसी चरित्र में सुखी लाला के रूप में वापस आए। लगभग पचास साल तक हिंदी फिल्मों की दुनिया में बने रहकर कन्हैयालाल ने ज्यादातर वही भूमिकाएं कीं जिन्हें वह स्वाभाविक रूप से कर लिया करते थे।

मोटे तौर पर कह सकते हैं कि टाइपकास्टिंग से उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं रही। फिल्मों में प्रायः ऐसे अभिनेता देर तक जमे रहते हैं जो दी गयी भूमिका को सीमित या निर्धारित समय में निभा कर ओके टेक दे दें। समझा जा सकता है कि इससे निर्माता निर्देशक किफायती ढंग से काम कर पाते हैं और सेट पर ज्यादा टेंशन भी नहीं होती। यह बात केवल अभिनेताओं ही नहीं बल्कि हर विभाग के प्रतिभागियों और कर्मचारियों पर लागू होती है।










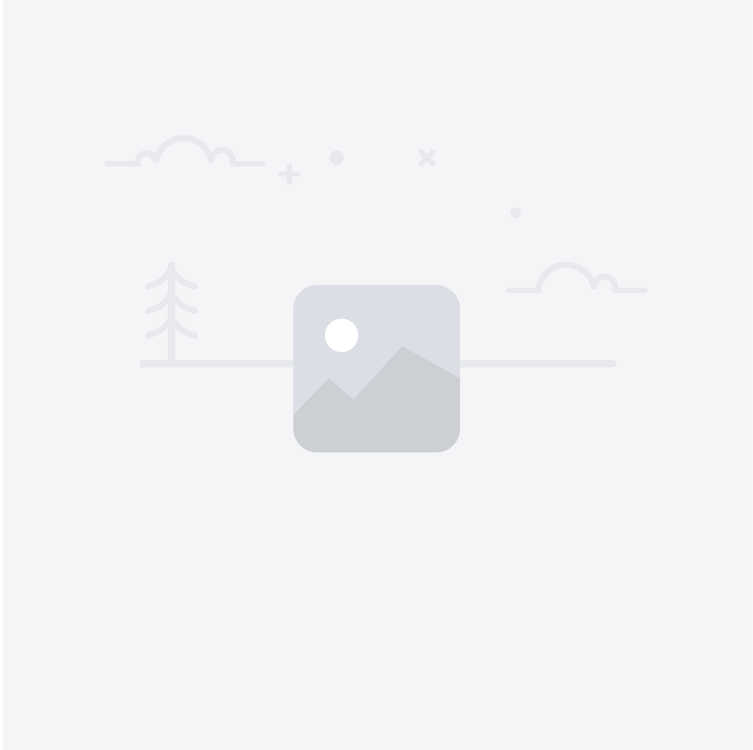










Write a comment ...